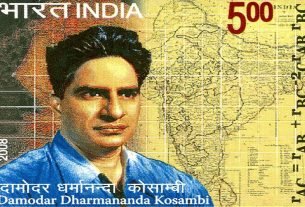यह वो दौर था जब मुघलिया सल्तनत का सूरज डूबने वाला था, बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत लाल क़िले की दीवारों के तक महदूद हो कर रह गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से लेकर कलकत्ता और बंबई से लेकर गुजरात तक भारत के एक बड़े हिस्से पर क़ब्ज़ा जमा लिया था।
कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी के सवाल पर भड़के फ़ौजी 10 मई 1857 को मेरठ में बग़ावत कर गए। बग़ावत के दौरान ग़ुस्से में भरे इन सिपाहियों ने जेल पर हमला करके वहाँ क़ैद आठ सौ अपराधियों, हत्यारों, जेबतराशों और दूसरे बदमाशों को भी आज़ाद कर दिया; जिनमें से अधिकतर लोग सिपाहीयों के साथ 11 मई 1857 को अपने घोड़े दौड़ाते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट के बाहर ब्रिगेडियर ग्रेव्स की सेना के सामने थे।
ब्रिगेडियर की सेना के ज़्यादातर सिपाहीयों ने पाला बदल लिया। बाक़ी बचे सिपाहीयों के साथ दिल्ली पर कब्ज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो गया। बाग़ी दिल्ली में दाख़िल हो गए। बहादुर शाह ज़फर की सुरक्षा में तैनात कप्तान डगलस और ईस्ट इंडिया कम्पनी के एजेंट साइमन फ्रेज़र को मार दिया गया। इस तरह बाग़ी सिपाही दिल्ली के लालक़िले पहुंच गए।
पढ़े : ‘1857 विद्रोह’ के बर्बर घटनाओं का दस्तावेज हैं ‘गदर के फूल’
पढ़े : मार्क्स ने 1857 के विद्रोह कि तुलना फ्रान्सीसी क्रांति से की थीं
क्या हुआ उस दिन?
अंग्रेज़ों की पेंशन पर गुज़ारा कर रहे और नाम भर के बादशाह रह गए, बहादुर शाह ज़फ़र के आगे गुहार की – “हे धर्मरक्षक, दीन के गुसैंया, हम धर्म और मज़हब को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से बग़ावत कर आए हैं। आप हमारे सिर पर हाथ रखें और इन्साफ़ करें। हम आपको भारत का शहंशाह बनाना चाहते हैं।”
और साथ ही बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से विद्रोह की अगुआई करने को कहा तो बूढ़े, हताश और दयनीय हो चुके बादशाह ने उनसे कहा –
“सुनो भाई! मुझे बादशाह कौन कहता है? मैं तो फ़क़ीर हूँ जो किसी तरह क़िले में अपने ख़ानदान के साथ रहकर एक सूफ़ी की तरह वक़्त गुज़ार रहा हूँ। बादशाही तो बादशाहों के साथ चली गई। मेरे पूर्वज बादशाह थे जिनके हाथ में पूरा भारत था। लेकिन बादशाहत मेरे घर से सौ साल पहले ही कूच कर गई है।”
बादशाह ने अपनी तंगहाली बयान की, “मैं अकेला हूँ। तुम लोग मुझे परेशान करने क्यों आए हो? मेरे पास कोई ख़ज़ाना नहीं है कि मैं तुम्हारी पगार दे पाऊँ। मेरे पास कोई फ़ौज नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके।
मेरे पास ज़मीनें नहीं हैं कि उसकी कमाई से मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकूँ। सल्तनत भी नहीं कि तुम लोगों को अमलदारी में रख सकूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझसे कोई उम्मीद मत करना। ये तुम्हारे और अँग्रेज़ों के बीच का मामला है।”
जवाब में बाग़ी सिपाहियों ने कहा “हमें यह सब कुछ नहीं चाहिए। हम आपके पाक क़दमों पर अपनी जान क़ुर्बान करने आए हैं। आप बस हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए।”
इसके बाद आकाशभेदी जयकारों व तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बहादुर शाह ज़फ़र एक बार फिर सचमुच के भारत के बादशाह और भारत की पहली जंगे आज़ादी के नेता बन गए। तोपख़ाने ने 21 तोपों दाग़कर उन्हें सलामी दी। इसके बाद बहादुर शाह के बेटे मिर्ज़ा ज़हीरउद्दीन दिल्ली में इस सिपाही सेना का कमांडर बनाए गए।
पढ़े : सिराज उद् दौला की वह माफी जिससे भारत दो सौ साल गुलाम बना
पढ़े : क्या कलासक्त होना था व़ाजिद अली शाह के गिरते वैभव कि वजह?
गालिब का नजरिय़ा
इस दौरान मशहूर उर्दू शायर मिर्ज़ा असदउल्लाह ख़ां ग़ालिब दिल्ली में ही थे। बग़ावत से पैदा हुए हालात पर उन्होंने अपनी किताब ‘दस्तंबू’ में कुछ यूं ज़िक्र किया है –
“11 मई, 1857 का दिन था, यकायक दिल्ली में हर तरफ़ होने वाले धमाकों से घरों के दरो-दीवार हिल गए। मेरठ के नमक हराम सिपाही अंग्रेज़ों के ख़ून से अपनी प्यास बुझाने दिल्ली आ पहुंचे थे। जिनके हाथों में दिल्ली की निगेहबानी थी वो भी जाकर बाग़ियों से मिल गये।
बाग़ियों ने पूरे शहर को रौंद डाला और उस समय तक अंग्रेज़ अफ़सरों का पीछा नहीं छोड़ा जब तक उन्हें क़त्ल न कर दिया। अंग्रेज़ बच्चे, ज़नानियां सब क़त्ल-औ-ग़ारत के शिकार हुए। लाल क़िले से बागियों ने अपने घोड़े बांध लिए और शाही महल को अपना ठिकाना बना लिया।
तीन दिन हो गए हैं, न पानी है और न ही कुछ खाने को। डाक का काम भी ठप्प हो गया है। मैं न दोस्तों से मिल पा रहा हूं और ना ही अपनों का हाल मालूम हो रहा है।”
यहां पर ग़ालिब जो बागियों को नमक हराम कहकर बुलाते हैं, उन्हीं के लिए आगे लिखते हैं, “ये हिम्मतवाले बाग़ी जहां से भी गुज़रे उन्होंने अपने क़ैदी साथियों को आज़ाद करा लिया।
इस समय दिल्ली के बाहर और भीतर कोई पांच हज़ार सैनिक जमे हुए हैं। गोरे अब भी हिम्मत जुटाए खड़े हैं। रात-दिन काला धुंआ शहर को लपेटकर रखता है। लुटेरे हर तरह से आज़ाद हैं। व्यापारियों ने टैक्स देना बंद कर दिया है, बस्तियां वीरान हो चुकी हैं।
बाग़ी सारा दिन सोना-चांदी लूटते हैं और शाम को महल के रेशमी बिस्तर पर नींद काटते हैं। शरीफ़ लोगों के घरों में मिट्टी का तेल भी नहीं है। हर तरफ़ अंधेरा है…”
चुंके बाग़ी सिपाहीयों के साथ अपराधियों, हत्यारों, जेबतराशों और दूसरे बदमाशों का हुजूम भी देल्ही पहुंच गया था। इस लिए अगले कुछ दिनों तक पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में अराजकता, लूट और हिंसा का बोलबाला रहा।
बहादुर शाह के एक दरबारी और शायर ज़हीर देहलवी ने इस आँखों देखे हालात और मंज़र को अपनी किताब ‘दास्तान-ए-ग़दर’ में कुछ इस तरह बयाँ किया है :-
जहाँ में जितने थे ओबाश रिंद ना फ़रजाम
दग़ाशियार, चुग़लख़ोर, बदमाश तमाम
हुए शरीक सिपाह-ए-शरर बद अंजाम
किया तमाम शरीफ़ों के नाम को बदनाम
इस बात से ज़ाहिर होता है, कि ज़हीर देहलवी सिपाहियों की बग़ावत से ख़ुश नहीं थे और न ही वो दिल्ली वालों की ज़िंदगी में अचानक आए एक तूफ़ान का इस्तक़बाल करने को तैयार थे। ज्ञात रहे के ‘दास्तान-ए-ग़दर’ में ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ हुई सिपाहीयों की बग़ावत का ब्यौरा दर्ज है।
पढ़े : अपनों की गद्दारी के चलते शहीद हुए तात्या टोपे
पढ़े : भगत सिंह ने असेम्बली में फेंके पर्चे में क्या लिखा था?
दास्तान-ए-ग़दर
इधर बरेली के नवाब बहादुर ख़ान के सेनापति बख़्त ख़ान ने जब बग़ावत की ख़बर सुनी तो बहादुर शाह ज़फ़र की मदद के लिए दिल्ली कि जानिब कूच करने को सोंचा।
पैदल और घुड़सवार सिपाहीयों कि सशस्त्र सेना की मदद से बरेली जेल में मौजूद सभी बंदियों को रिहा कराया और ख़ज़ाने पर क़ब्जा़ कर लिया। साथ ही इस दौरान रुहेलखंड को बाग़ियो के नियंत्रण में रखा और अपने मार्गदर्शक मौलवी सरफ़राज़ अली के साथ अंग्रेज़ों से दिल्ली को बचाने के लिए कूच किया।
1 जुलाई 1857 को बख़्त ख़ान पीपे के पुल से दिल्ली पहुँचे जहां उनका इस्तक़बाल बेगम ज़ीनत महल के पिता नवाब अली ख़ान ने किया। चूँकि इतनी बड़ी फ़ौज को दिल्ली में रखा नहीं जा सकता था, इसलिए दिल्ली गेट के बाहर रखा गया। यह इसलिए भी ज़रुरी था क्योंकि सिपाही पहले से ही पबरे शहर, घर एवं बाज़ार में छाये हुए थे।
बूढ़े और कमज़ोर शहंशाह बहादुर शाह ने बख़्त ख़ान और उनके सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हुए उनको साहिब-ए-आलम का लक़ब दिया। अपने बेटे की जगह बख़्त ख़ान को सबसे बड़ा ओहदा दिया और सेनापति बनाया। सम्राट ने अपने पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल को उसके ज़ेर ए निगरानी रखा। बख़्त ख़ान को गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई।
अपने पहुँचने के एक सप्ताह के भीतर बख़्त ख़ान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उसने शाही स्टाफ़ को वेतन देने का आदेश दिया, और जिन सैनिकों ने लूटपाट की थी उन्हें गिरफ़्तार कर सज़ा देने का आदेश दिया। बाज़ार ख़ाली करके सैनिकों को दिल्ली गेट के बाहर किया गया। फ़ौज को तीन हिस्सों में बाँट दिया गया, जिसके एक हिस्से को रोज़ लड़ाई में मशग़ूल रखा गया।
19 जुलाई 1857 को बख़्त ख़ान और उसके सिपाही पश्चिम की ओर गए और चौकियों पर क़ब्ज़ा कर लिया। पर ये क़ब्ज़ा अधिक दिनो तक नही रहा और 20 सितंबर, 1857 को ब्रितानी सेनाओं ने भारतीय बाग़ियों को हराकर दिल्ली पर दोबारा क़ब्ज़ा कर लिया।
पढ़े : जब अपने दोस्त जगन्नाथ के हाथों काटे गये क्रांति योद्धा अहमदुल्लाह
पढ़े : ‘देहली कॉलेज’ ब्रिटिशों के खिलाफ करता रहा अस्तित्व का संघर्ष
और शहंशाह हुए दर बद़र
भारतियों की मिली हार के बाद शहंशाह बहादुर शाह ने अपना क़िला छोड़कर उस समय दिल्ली शहर के बाहर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सराय के पास मौजूद हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। दिल्ली में भारती सेना के सेनापति जनरल बख़्त ख़ान ने लाल क़िला छोड़ने से पहले बादशाह को अपने साथ चलने के लिए कहा था।
बख़्त ख़ान ने बादशाह से कहा था, “हालांकि ब्रितानियों ने शहर पर क़ब्ज़ा कर लिया है लेकिन भारती सेना के लिए ये उतना बड़ा सदमा नहीं है क्योंकि इस वक़्त पूरा भारत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है और हर कोई रहनुमायी के लिए आपकी तरफ़ देख रहा है। आप मेरे साथ पहाड़ों की तरफ़ चलें, वहां से लड़ाई जारी रखी जा सकती है। वहां अंग्रेज़ों के लिए हमारा मुक़ाबला करना संभव नहीं होगा।”
बहादुर शाह ज़फ़र को बख़्त ख़ान की बात सही लगी। उन्होंने ख़ान को अगले दिन हुमायूं के मकबरे पर मिलने के लिए कहा। पर अंग्रेज़ों के मुख़बिर मिर्ज़ा इलाही बख़्श और मुंशी रज्जब अली ने उन दोनों की बातचीत की ये ख़बर अंग्रेजों तक पहुंचा दी और धोखे से बादशाह को दिल्ली में रुकने के लिए मना लिया। नतीजतन, बादशाह को हडसन ने गिरफ़्तार कर लिया, उनपर मुक़दमा चलाया गया और सज़ा के तौर पर उन्हें जिला वतन कर रंगून भेज दिया गया।
पढ़े : शायरी कि बारीकियां सिखाते गालिब के कुछ खत
पढ़े : मिर्जा ग़ालिब अपने ही शायरी के थे आलोचक
थाल में मिला बेटों का सर
मुक़दमे के दौरान बहादुर शाह के सामने थाल लाया गया। हडसन ने तश्त पर से ग़िलाफ़ हटाया। कोई और होता तो शायद ग़श खा जाता या नज़र फेर लेता। लेकिन बहादुर शाह ने ऐसा कुछ नहीं किया। थाल मे रखे जवान बेटों के कटे सिरों को इत्मीनान से देखा।
हडसन से मुख़ातिब हुए और कहा – “वल्लाह… नस्ले ‘तैमूर’ के चश्मो चराग़ मैदाने जंग से इसी तरह सुर्ख़रू होकर अपने बाप के सामने आते हैं। हडसन तुम हार गए और भारत जीत गया।”
यह बात क़ाबिल ए ज़िक्र है के बहादुर शाह अपने सलतनत के आख़री दिन तक ख़ुद को नस्ल ए तैमूर यानी तैमूर वंश का मान रहे थे।
ज्ञात रहे के लाला क़िला छोड़ कर बहादुर शाह सीधे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे थे और वहां उनकी मुलाक़ात ख़्वाजा शाह ग़ुलाम हसन से हुई थी; जिन्हे बहादुर शाह ने बताया, “मुझे कुछ समय पहले ही लग गया था कि मैं गौरवशाली तैमूर वंश का आख़री बादशाह हूं।
अब कोई और हाकिम होगा। उसका क़ानून चलेगा। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है, आख़िर हमने भी किसी और को हटाकर गद्दी पायी थी।”
बादशाह ने उनसे आगे बताया कि जब तैमूर ने क़ुस्तुनतूनिया (तुर्की का एक ऐतिहासिक शहर इस्तांबोल) पर हमला किया, तब उन्होंने वहाँ के पुराने सुल्तान बा यज़ीद यलदरम से पैगम्बर मुहंमद (स) के ‘दाढ़ी का बाल’ हासिल किया था।
जो अब तक मुघल बादशाहों के पास महफ़ूज़ था लेकिन “अब आसमान के नीचे या ज़मीन के ऊपर मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है इसलिए मैं इस अमानत को आपके हवाले कर रहा हूं ताकि यह महफ़ूज़ रहें।”
ख़्वाजा शाह ग़ुलाम हसन ने ज़फर से वह बाल ले लिए और उन्हें दरगाह की तिजोरी में रख दिया।
एक दिन से भूखे बादशाह बहादुर शाह यहां केवल पैगम्बर मुहंमद (स) के पवित्र अवशेष सौंपने और आशीर्वाद लेने के लिए आए थे; जिसके बाद बादशाह हुमायूं के मक़बरे में चले गए।
पढ़े : बेशर्म समाज के गन्दी सोंच को कागज पर उतारते मंटो
पढ़े : कैफ़ी ने शायरी को इश्कियां गिरफ्त से छुड़ाकर जिन्दगी से जोड़ा
भेजे गए रंगून
मुघल बादशाह बहादुर शाह के क़ैद हो जाने के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली को ख़ाली करवा लिया था। अंग्रेज़ों के सिवाय यहां कोई नहीं था। इसके 15 दिन बाद हिन्दुओं को दिल्ली लौटने और रहने की इजाज़त दे दी गई। दो महीने बाद मुसलमानों को भी दिल्ली आने की अनुमति मिली, लेकिन इसमें बड़ी शर्त थी।
इस शर्त के मुताबिक, मुसलमानों को दरोग़ा से परमिट लेना था। इसके लिए दो आने का टैक्स हर महीने देना पड़ता था। थानाक्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। रक़म न देने पर दरोग़ा के आदेश पर किसी भी इंसान को दिल्ली के बाहर धकेल दिया जाता था।
वहीं, हिन्दुओं को इस परमिट की जरूरत नहीं होती थी। कुछ ऐसा ही मिर्ज़ा ग़ालिब के साथ भी हुआ। वो दिल्ली में हर महीने दो आने अंग्रेजों को देते थे। पुस्तक ‘ग़ालिब के खत किताब’ में ग़ालिब ने इस परेशानी का ज़िक्र का किया है।
मिर्ज़ा ग़ालिब ने जुलाई 1858 को हकीम ग़ुलाम नजफ़ ख़ां को ख़त लिखा था। दूसरा ख़त फ़रवरी 1859 को मीर मेहंदी हुसैन नज़रू शायर को लिखा था। दोनों ख़त में ग़ालिब ने कहा है, “हफ़्तों घर से बाहर नहीं निकला हूं, क्योंकि दो आने का टिकट नहीं ख़रीद सका।
घर से निकलूंगा तो दारोग़ा पकड़ ले जाएगा।” ग़ालिब ने दिल्ली में 1857 की क्रांति देखी। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह का ज़वाल देखा। अंग्रेज़ों का उत्थान और देश की जनता पर उनके ज़ुल्म को भी गालिब ने अपनी आंखों से देखा था।
वो लिखते हैं –
अल्लाह! अल्लाह!
दिल्ली न रही, छावनी है,
ना क़िला, ना शहर, ना बाज़ार, ना नहर,
क़िस्सा मुख़्तसर, सहरा सहरा हो गया।
कितना बदनसीब है ज़फर…
इधर 17 अक्टूबर 1858 को बाहदुर शाह ज़फर मकेंजी नाम के समुंद्री जहाज़ से शाही ख़ानदान के 35 लोग के साथ रंगून पहुंचा दिए गये। कैप्टेन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था, उसने बादशाह और उसके लोगों को बंदरगाह पर रिसीव किया और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह को लेकर अपने घर पहुंचा।
बहादुर शाह ज़फर क़ैदी होने के बाद भी बादशाह थे, इसलिए नेल्सन परेशान था, उसे ये ठीक नही लग रहा था कि बादशाह को किसी जेल ख़ाने में रखा जाए… इसलिए उसने अपना गैराज खाली करवाया और वहीं बादशाह को रखने का इंतज़ाम करवाया।
बहादुर शाह 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में गए और 7 नवंबर 1862 को अपनी चार साल की गैराज की ज़िन्दगी को मौत के हवाले कर के ही निकले , बहादुर शाह ज़फर ने अपनी मशहुर ग़ज़ल इसी गैराज में लिखा था –
लगता नही है दिल मेरा उजड़े दियार में
किस की बनी है है आलम न पायेदार में
और
कितना बदनसीब है ज़फर दफ़न के लिए
दो गज़ ज़मीन भी न मिले कुए यार में..
7 नवंबर 1862 को बादशाह की ख़ादमा परेशानी के हाल में नेल्सन के दरवाज़े पर दस्तक देती है, बर्मी खादिम आने की वजह पूछता है, ख़ादमा बताती है बादशाह अपनी ज़िन्दगी के आख़री साँस गिन रहा है गैराज की खिड़की खोलने की फ़रमाईश ले कर आई है।
बर्मी ख़ादिम जवाब में कहता है, अभी साहब कुत्ते को कंघी कर रहे हैं। मै उन्हें डिस्टर्ब नही कर सकता। ख़ादमा जोर जोर से रोने लगती है। आवाज़ सुन कर नेल्सन बाहर आता है। ख़ादमा की फरमाइश सुन कर वो गैराज पहुँचता है।
बादशाह के आख़री आरामगाह में बदबू फैली हुई थी और मौत की ख़ामोशी थी.. बादशाह का आधा कम्बल ज़मीन पर और आधा बिस्तर पर… नंगा सर तकिये पर था लेकिन गर्दन लुढ़की हुई थी.. आँख को बहार को थे.. और सूखे होंटो पर मक्खी भिनभिना रही थी।
नेल्सन ने ज़िन्दगी में हज़ारो चेहरे देखे थे लेकिन इतनी बेचारगी किसी के चेहरे पर नही देखी थी। वो बादशाह का चेहरा नही बल्कि दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा था। उसके चेहरे पर एक ही फ़रमाइश थी। आज़ाद साँस की !
भारत के आख़री बादशाह की ज़िन्दगी खत्म हो चुकी थी। कफ़न दफ़न की तय्यारी होने लगी। शहजादा जवान बख़्त और हाफिज़ मुहंमद इब्राहिम देहलवी ने गुसुल दिया। बादशाह के लिए रंगून में ज़मीन नही थी। सरकारी बंगले के पीछे खुदाई की गयी। और बादशाह को खैरात में मिली मिटटी के निचे डाल दिया गया।
उस्ताद हाफिज़ इब्राहिम देहलवी के आँखों को सामने 30 सितम्बर 1837 के मंज़र दौड़ने लगे। जब 62 साल की उम्र में बहादुर शाह ज़फर तख़्त नशीं हुआ था, वो वक़्त कुछ और था.. ये वक़्त कुछ और था…. इब्राहिम दहलवी सुरह तौबा की तिलावत करते है, नेल्सन क़बर को आख़री सलामी पेश करता है … और एक सूरज ग़ुरूब हो जाता है।
जाते जाते :
लेखक हेरिटेज टाइम्स के संपादक हैं।