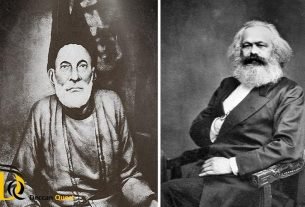हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान के आधुनिक हिमायती यह जान कर बेहोश न हों कि भाषा के लिए हिन्दी शब्द के सबसे पहले उपयोग का श्रेय हिन्दुओं को नहीं, मुसलमान लेखकों और कवियों को जाता है। अमीर खुसरो की ‘खालिक बारी’ हिन्दी-उर्दू का सबसे पुराना कोष है।
इसमें बारह बार हिन्दी और पचपन बार हिन्दवी शब्द का उपयोग मिलता है। दोनों शब्दों का सीधा मतलब है हिन्द, यानी भारत के सभी निवासियों की भाषा। इन दोनों शब्दों के बीच जुड़ाव का सूचक (याय निस्बती) ईकार है।
शाह हातम अपने ‘दीवानजादे’ की भूमिका में लिखते हैं कि हिन्दवी जिसे भाखा भी कहते हैं, आम लोग भी बखूबी समझते हैं और बड़े तबके के लोग भी। तुलसीदास ने भी इस भाषा के लिए भाखा शब्द ही इस्तेमाल किया है (भाखा भनति मोर मति थोरी)।
18वीं सदी में उर्दू भाषा के लिए रेख्ता लफ्ज भी मिलता है जो कवि समाज में फारसी के बरक्स उर्दू कविता के पढ़े जाने (मराख्ता) से निकला है। मूल मतलब है – हिन्द में तमाम आसपास की बोली जाने वाली बोलियों से घुलमिल कर बनी जुबान। उर्दू कवियों में इस जुबान के महारथी मीर को माना जाता है जिनको परवर्ती गालिब ने भी सलाम किया है-
‘रेख्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो ‘गालिब’
कहते हैं अगले जमाने में कोई ‘मीर’ भी था।’
पढ़े : क्या हिन्दोस्ताँनी जबान सचमूच सिमट रही हैं?
पढ़े : मज़हब की बंदिशों से आज़ाद उर्दू ग़ज़ल
पढ़े : जब तक फिल्मे हैं उर्दू जुबान जिन्दा रहेंगी
गलतफहमी की जड़
18वीं सदी के भारत में लिखना-पढ़ना या तो पंडित वर्ग करता था या फिर दरबार से जुड़े सरकारी कर्मचारी जिनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। बाकी समाज में साक्षरता दर बहुत कम थी। 19वीं सदी की शुरुआत में जॉन गिलक्राइस्ट ने जनता तक राजकीय निर्देश पहुंचाने और सरकारी राजकाज के निचले तबके के लिए मुदर्रिस मुंशी तैयार करने की नीयत से लिखित मानक भाषा रचने का काम चार भाखा मुंशियों को थमाया।
हुकूम था कि साक्षरता तेज हो और स्कूली प्रणाली में फारसी से जुड़ी उर्दू को मुसलमानों की और संस्कृत से जुड़ी हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा मान कर पाठ्य पुस्तकों को दो अलग लिपियों में लिखाया-पढ़ाया जाए। भाषा मुंशियों ने इसी हुकुम तले जनभाषा को लिपि के आधार पर दो फाड़ कर दिया। लिपि का यही मुद्दा हिन्दी-उर्दू-हिन्दवी या हिन्दुस्तानी को अलग-अलग संप्रदायों की भाषाएं मानने की गलतफहमी की जड़ बनता चला गया।
किसी भी मिले-जुले समाज में बोलचाल की भाषा खुद में धर्मनिरपेक्ष होती है। पर जबरन बांटे गए दो धार्मिक संप्रदायों के बीच भाषा की सीमा रेखा पर गरमी बढ़ना हर संप्रदाय को पुराने सामाजिक समन्वय, सह-अस्तित्व की जगह अपने-अपने धार्मिक और जातीय इतिहास की तरफ पक्षपाती बना देता है।
ठीक इसी समय भारतीय समाज के बीच पश्चिमी हवाएं यूरोप से लगातार परंपरा, संस्कृति, देशभक्ति और राष्ट्रीयता की बाबत नए विचार ला रही थीं। इसका फायदा यह हुआ कि भाषा का मसला नाहक हिन्दू पहचान, मुस्लिम पहचान का मसला बन गया।
पढ़े : अनुवाद में कठिन शब्दों को निकालने कि ‘आज़ादियां’ है
पढ़े : अनुवाद में मूल भाषा का मिज़ाज क्यों जरुरी हैं?
पढ़े : भारतीय भाषाओं में कुऱआन के अनुवाद का रोचक इतिहास
राजनीति का हथियार
फिर भी 20वीं सदी तक दोनों भाषाओं के बीच ताक-झांक साहब-सलामत रही। भाषा के इस सर्वधर्मसमभावी महत्त्व को गांधी ने पहचाना और अपने तीन भाषाई अखबारों (हिन्दी में नवजीवन और गुजराती में कौमी आवाज) तथा प्रार्थना सभाओं की मार्फत भारत की अवाम तक सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे।
अफसोस कि लोकभाषा और लोकमानस ने पिछली आठ सदियों में बार-बार एक बोलचाल की जनभाषा से जो ताकतवर बवंडर तैयार किया, उसका फायदा हमारा नवसाक्षर समाज नहीं उठा पाया। फारसी गई तो अंग्रेजी आई। जनता की जुबान जो हिन्दी-उर्दू भाषाएं देश में राजनीति, सामाजिक सुधार और समन्वयवाद पर बतकही के लिए खुली व्यापक जमीन तैयार कर सकती थीं, प्रतिगामी राजनीति का हथियार बन गईं।
पाकिस्तान को इस मनमुटाव की सजा मिली कि पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी और बलूची बोलने वालों ने उर्दू को मुहाजिरों की भाषा कह कर उसे राजभाषा नहीं बनने दिया। उधर, उत्तर भारतीय राजनेताओं की कांइयां राजनीति और सवर्णमूलक सांप्रदायिक चुनाव प्रचार से नाराज अहिन्दीभाषी राज्यों ने हिन्दी के लिए भी भारत की राजभाषा बनने का रास्ता बंद करा दिया। सीमा के आर-पार सत्ता, नौकरशाही, रुतबेबाजी और महत्वाकांक्षा की भाषा अंग्रेजी ही बनी रही और अल्गोरिद्म-चालित नेट के युग में आगे भी काफी समय तक बनी रहेगी।
पढ़े : उर्दू और हिन्दी तरक्की पसंद साहित्य का अहम दस्तावेज़
पढ़े : आज़ादी के बाद उर्दू को लेकर कैसे पैदा हुई गफ़लत?
पढ़े : गुरुमुखी लिपि हिन्दी अक्षरों का बिगड़ा हुआ रूप
भाषाई सामाजिक यथार्थ
विजयदेव नारायण साही की मानें तो गालिब और मीर के बाद के शायर और मंटो के बाद के लेखक पाकिस्तान में उर्दू की दुनिया के स्थायी वासी नहीं बने। न ही हिन्दी के लेखक भारतीय राजनीति में कोई बदलाव ला सके। इस बीच मिडनाइट्स चाइल्ड सलमान रुश्दी, हनीफ कुरेशी, आतिश तासीर, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, आलोक राय या राम गुहा तक आज के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चर्चित लेखकों की एक लंबी फेहरिस्त है, जो अब अपनी मातृभाषा में सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ पर अंग्रेजी में ही लिखना पसंद करते हैं।
पिछली आधी सदी में सत्ता पक्ष से चिपक कर हिन्दी हिन्दुत्ववादी और अपनी अविनाशी सत्ता के छलावे में डूबी, ‘बाहरी’ शब्दों के जबरन विरेचन को व्याकुल होकर उर्दू के साथ अपनी ही शब्द संपदा का भी संहार करने पर तुली नजर आती है।
निराला या गालिब की संयत वेदना, प्रसाद या महादेवी की शांत आत्मलीनता, छोटे शहरों के बुझे जाते निचले वर्गों की वेदना उकेरने वाले मुक्तिबोध, रामकुमार, कमलेश्वर और भारती, अपने व्यंग्य में भी अपनी जमीन के लोगों के लिए डबडबाई आत्मीयता रचने वाले शरद जोशी, परसाई धीमे-धीमे समय के कुहासे में लोप हो रहे हैं।
एक खास शहरियत का तेवर पाने के लिए सोशल मीडिया पर भी हिन्दी-उर्दू, दोनों ने गांवों तक फैले बोलियों में बोलने वाले भारत से खुद को लगता है काट लिया है। कहते हैं, खजुराहो में किसी गाइड ने किसी विदेशी सैलानी को समझाते हुए कहा, ‘जी, ये असली मंदिर नहीं जहां पूजा होती है, ये तो बस भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं।’
सो, पाठक बुरा न मानें लेकिन हिन्दी पत्रकारिता से साहित्य तक हिन्दी-उर्दू के हमारे लेखक समाज से कस कर जुड़े हुए स्थायी भाषा साधक नहीं रहे। न ही वे लिपि, राजनीति या धर्म के मसलों में उलझी भारतीय संस्कृति को ठीक करने की मंशा रखते हैं।
वे भाषा के सैलानी हैं जो थोड़ी देर के लिए पर्यटकों को अपने इलाके में लाकर उनको दूरबीन से स्थापत्य निहारने लायक मसाला जुटाते हैं। पर पर्यटकों की पीठ फिरी नहीं कि वे अपने लिए अंग्रेजी छापे की दुनिया से तगड़े गाहक जुटाने को चल देते हैं।
(यह लेख मूल रूप से नवजीवन में प्रकाशित हुआ हैं)
जाते जाते :