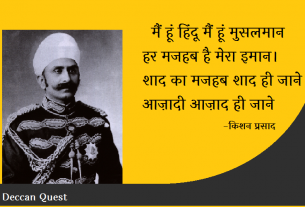एक्शन किंग निर्देशक रोहित शेट्टी इस बात का रोना रो रहे हैं कि सोशल और प्रिंट मीडिया में उन पर यह तोहमत लगाई जा रही है कि उनकी फिल्म ‘सूर्यवशीं’ के खलनायक मुसलमान हैं। वह इस पर जवाब में कहते हैं, “आज से पहले मुझसे ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा ही नहीं?”
वह एक पेचीदा स्पष्टीकरण के साथ जोर देकर कहते हैं कि उनकी ‘सिंघम’, ‘सिंघम रिटर्न्स’ और ‘सिम्बा’ में उनके सभी हिंदू किरदार भी ‘नकारात्मक ताकतें’ थे। ठीक है। इस बिंदु पर ज्यादा उपयुक्त प्रश्न यह है, “श्रीमान शेट्टी, यह परिवर्तन क्यों?”
इसके अलावा, वह अपनी सुविधा के हिसाब से यह उल्लेख करना भूल जाते हैं कि उनकी पहली फिल्म ‘जमीन’ (2003) में जो दुश्मन था, वह एक वहशी चरमपंथी नेता जहीर खान था। इसलिए, इस मसले को यहीं छोड़ देते हैं।
यह विडंबना ही है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी अनिल शर्मा की फिल्म ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’ (2004) में एक इस्लामी कट्टरपंथी की भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया था।
उनका तर्क था कि इससे उनके मुस्लिम प्रशंसक नाराज हो जाएंगे। और यहां उनकी भूमिका पूरी तरह से बदल दी गई। इसमें वह दुश्मन के शिविर में एक युद्धबंदी के रूप में हैं।
जैसा कि बॉलीवुड फिल्मों का एक आजमाया फॉर्मूला है कि पटकथा में कुछ किनारे के पात्रों में गुणी और वीर मुसलमान चरित्र अभी भी रखते जाते हैं। ठीक जैसे कि 1950 और 1960 के दशक में बनी फिल्मों में यह अनिवार्य था कि उसमें एक दयालु रहीम चाचा और एक जुलेखा दाई मासी वफादार घरेलू मददगार के रूप में होते ही थे।
पढ़े : फिल्म इंडस्ट्री के ‘क्लब क्लास’ को जिम्मेदार बनना होगा
पढ़े : मणि कौल ने फिल्मों से पैसा नहीं बल्कि नाम कमाया
पढ़े : सिनेमा को बुराई कहने पर गांधी पर उखडे थे ख्वाजा अहमद अब्बास
नकारात्मक चित्रण
यह तो स्वाभाविक है कि सिनेमा को अपने समय की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करना होता है। अगर एक समय में माफिया डॉन, हर रंग के स्मगलर और उनके साथ कानूनी बल के भ्रष्ट तत्व तथा लालची राजनेता मुख्य शत्रु होते थे, तो इसका भी कारण है कि चरमपंथीयों के किरदार या तो अतिकाल्पनिक होते हैं या भी फिर सच्ची घटनाओं से प्रेरित होते हैं।
लेकिन वे आज की फिल्मों की कहानियों का बहुत ही आंतरिक हिस्सा होते हैं। लेकिन जो आपत्ति है, वह यह है कि अक्सर पूरे मुस्लिम समुदाय को एक ही काले रंग से पोत दिया जाता है। अंधराष्ट्रवाद, अविश्वसनीय और पूर्वानुमान वाले आख्यानों का इस्तेमाल सिर्फ आस्थाओं के बीच विभाजन को ही बढ़ाता है।
शुक्र है कि दशकों से कम-से-कम कुछ मुट्ठीभर फिल्मकार रहे हैं जिन्होंने इस विषय को बहुत ही सयंमित तरीके संभाला और उन कारणों को तलाशा है जिनकी वजह से अनगिनत लोगों की जानें गई है।
इनमें से सबसे प्रमुख उदाहरण हैं मणि रत्नम की ‘रोजा’ (1992), ‘बॉम्बे’ (1995) और ‘दिल से’ (1998), गुलजार की ‘माचिस’ (1996), अनुराग कश्यप की ‘ब्लैक फ्राइडे’ (2005), निशिकांत कामत की ‘मुंबई मेरी जान’ (2008), नीरज पांडेय की ‘अ वेन्ज्डे’ (2008), विशाल भारद्वाज की ‘हैदर’ (2014) और अनुभव सिन्हा की ‘मुल्क’ (2018)।
अगर मोटा-मोटी देखें तो मौजूदा समय में मुसलमानों पर केन्द्रित विषय वे हैं जिन पर शायद पहले कभी भी प्रयास नहीं किया गया। और वे फिल्म में होते भी हैं तो वही घिसे-पिटे अंदाज में, उनके घरों की दीवारों को हरे रंग से रंग दिया जाता है।
‘नमाज’ का एक दृश्य तो जरूर ही होता है और बुजुर्ग पुरुषों को गोल टोपी पहने एवं औरतों को दुपट्टे से अपना सिर ढके हुए दिखाया जाता है। और 2019 में बनी जोया अख्तर की ‘गली बॉय’ को ही ले लें; प्रगतिशील मुस्लिम लड़की का किरदार निभा रही आलिया भट्ट भी हिजाब ओढ़े हुए होती हैं।
पढ़े : साहिर लुधियानवी : फिल्मी दुनिया के गैरतमंद शायर
पढ़े : हसरत जयपुरी का गीत ना बजे तो भारत में कोई शादी पूरी नही मानी जाती
पढ़े : शकील बदायूंनी : वो मकबूल शायर जिनके लिये लोगों ने उर्दू सीखी
मेरी पटकथा नहीं बिकती
सन 2000 में बनी ‘फिजा’ और सन 2003 में बनी ‘तहजीब’ (जिनमें समकालीन मुसलमानों को सामान्य लोगों की तरह दिखाया गया है जो रोजमर्रा की दुविधाओं से जूझ रहे थे, यह बहुत आशावादी था) के बाद अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझे अपनी बाद की लिखी गई पटकथाओं के लिए धन जुटाना बहुत ही असंभव हो गया।
मुझे आमतौर पर इस व्यवसाय के दिग्गजों द्वारा यह कहा गया कि “अपने नायक ‘रियाज’ को ‘राहुल’ बना दो और अपनी नायिका ‘नीलोफर’ को ‘नीता’ बना दो, तब हम आगे बात करेंगे।”
कारण अपने आप में साफ था। चौदहवीं का चांद (1960), मेरे महबूब (1963) और निकाह (1982) में जिस स्तर पर मुस्लिम सामाजिक परिवेश को दिखाया गया था, वह बाद में विलुप्त हो गया और इस पर बॉलीवुड का कहना है कि इस प्रकार की फिल्मों का प्रस्ताव कैश काउंटर पर काफी जोखिम भरा हो जाता है।
करण जौहर को इस बात का श्रेय तो देना ही चाहिए कि उन्होंने दो समुदायों के बीच ध्रुवीकरण के मुद्दे को ‘माई नेम इज खान’ (2010) में संबोधित किया, हालांकि इसकी वजह से एक बहुत ही कटु राजनीतिक विवाद शुरू हुआ जिसके चलते घरेलू बॉक्स ऑफिस पर क्लेक्शन को नुकसान हुआ।
लेकिन विदेशों में इस फिल्म को जिस तरह स्वीकारा गया, उसके चलते इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विदेशों में इस फिल्म ने उस समय 33.5 मिलियन डॉलर का जबरदस्त कारोबार किया।
वास्तव में यह बात तो स्पष्ट है कि वे कमाल अमरोही की ‘पाकिजा’ (1972) या एमएस सथ्यूकी ‘गर्म हवा’ (1973) जैसी फिल्में अब नहीं बनाते हैं। हर पीढ़ी के फिल्मी दर्शक इस बात से अवगत हैं कि हाल के दशकों में सिनेमा में विषयगत गिरावट तो आई है बल्कि वर्तमान में जो मंत्र है, वह तो यह है कि तेलुगु, मलयालम और तमिल की सफल फिल्मों के रीमेक बनाए जाएं।
अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्क्रीन पर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को कुछ बहुत ही अशिष्ट तरीके से दिखाया जाता है और यह अस्वीकार्य है। वास्तव में आज सिनेमा को छोटे-मोटे खूंटे गाड़ ने के बजाय एक सर्वरोगहरण औषधि की जरूरत है।
यह आवश्यक है कि पात्र जैविक रूप से कथानक से ही उभर कर आए, जाति, संप्रदाय और धर्म की कोई रोक न हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हैं तो। जब तक फिल्मकारों को अपनी कहानी पर पूरा विश्वास है और उन्हें यह भरोसा है कि इसे जरूर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो तय है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
तब तक, ऐसे खंडन कि “मेरी पिछली फिल्मों में हिंदू खलनायक थे”, उतना ही खोखला सुनाई देता है जितना कि चुनाव से पहले किए गए वायदे।
जाते जाते :
* एक अफवाह ने दिलाई थी अताउल्लाह ख़ान को शोहरत
* जब तक रफी के गीत नही होते, हिरो फिल्में साईन नही करते!
*सूर और ताल की सौगात पेश करने वाले नौशाद अली
लेखक फिल्मकार हैं, उन्होंने झुबैदा, फिजा, तहजीब जैसे मुस्लिम परिवेश के फिल्मों का निर्माण किया हैं।